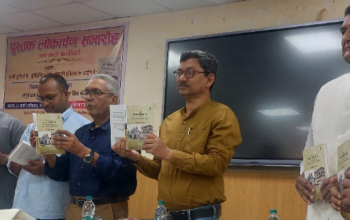होश संभालते ही देखा शीशम के खम्भे पर टिका फूस का घर । बाहर से टाटी से घिरे घर के दरबाजे पर शीशम के मोटे तख्ते से बनी अनगढ किवाड़। किबाड़ को अंदर से बंद करने के लिए सिटकिनी और बाहर से बंद करने के लिए जंजीर । घर का छप्पड़ पतले बांस, ईंकड़ी और खढ़ से बनता था। कुछलोग इसके ऊपर से खपड़ा भी डाल देते थे। कहते थे खपरैल घर गर्मी में ठंढा होता है।गांव में इक्के-दुक्के घर भित्ती वाले भी थे। भित्ती माने मिट्टी की 30-40 इंच मोटी और काफी ऊंची दीवार । काफी ऊंचाई पर छोटी-सी खिड़की होती थी। गांव में दो घर छतदार भी थे। उन्हें तब काफी सम्पन्न माना जाता था। मगर आजादी की लड़ाई इन पक्का घर वालों ने नहीं, फूस और भित्ती के घरवालों ने ही लड़ी थी ।

मैं कभी भित्ती और पक्का वाले घरों के भीतर नहीं गया। इसलिए उसके बारे में कुछ खास नहीं बता सकता। फूस के घर में मेरी पैदाईश हुई और जवानी भी उसी घर में बीती। इसलिए उसके जर्रे-जर्रे से परिचित हूं। बंसवारी, खढौरी, ईंकड़ी का खेत और शीशम का बगीचा अपना था। झलसी के पौधे से अगहन-पूस महीने में मूंज निकाला जाता और फिर झलसी की कटाई हो जाती थी। इस झलसी को सुखा कर मवेशी का बथान बनाया जाता और मूऔज से रस्सी बांट कर घरछौनी कराई जाती थी। तीन साल पर छप्पड़ की ऊपरी सतह का खढ़ हटा कर नये खढ़ से छाने का काम होता था। इसी को घरछौनी कहते थे। घर छाने वाले मजदूर को घरामी कहा जाता था। उसका दो ही औजार होता था- अंकुसा और पघरिया। अंकुसा लोहे की पत्ती या पतले छड़ की अर्धचंद्राकार आकृति वाला औजार को कहते हैं। इसमे मूंज की रस्सी का एक सिरा घुसा कर छप्पड़ के नीचे वाली बत्ती ( फट्टी ) से खढ़ के ऊपर वाले खढ़बत्ती को खूब कस कर बांधा जाता था। 12 से 15 इंच पर एक बंधन पूरी ताकत लगा कर खढ़ को खींचिए लेकिन क्या मजाल कि एक इंच भी खढ़ खिंच जाए। छप्पड़ के कोरों से पटुआ की रस्सी का सिकहर घर के अंदर लटका रहता था। हर कोठरी में दो-दो, तीन-तीन सिकहर पर माटी की कोही में दही, मक्खन, घी और हंडिया में रंग-विरंग का अचार। रस्सी का महीन जालीदार जल्ला भी सिकहर  की तरह लटका रहता था जिसमें लोग प्याज रखते थे।
की तरह लटका रहता था जिसमें लोग प्याज रखते थे।
ओसारे के एक कोना में ऊखल और अलगनी बनाकर दो-चार मूसल भी रखा रसता था। ओसारे के दूसरे किनारे पर स्थाई रूप से गाड़ा हुआ जांता और उससे कुछ दूर पर छोटी चकड़ी भी थी। जांता में आंटा पीसा जाता और चकड़ी से अरहर, मूंग, मसूर की दाल बनाई जाती थी। अगहन में जब धान की फसल तैयार हो जाती तब धान को उसन कर दो दिन तक सुखाया जाता फिर बोरा में रखकर दो-चार दिन छोड़ दिया जाता। इसके बाद ओखल में धान की कुटाई होती, छंटाई होती थी। तब एक बार धान कूटने को बोकरा और उसे फिर दुबारे कूटने को छंट्टा कहते थे। छंट्टा वाला चावल ही खाया जाता था। तैयार चावल माटी की कोठी में संजो कर रखा जाता। कोठी के नीचे धान कुट्टी का महीन भूंसा फिर उसके ऊपर चावल बांस के सूप में भर-भर पर कोठी में ऊपर से गिराया जाता। कोठी भर जाती तो उसका नीचे और ऊपर वाला मुंह मिट्टी वाले ढक्कन से गीली मिट्टी के की सहायता से बंद कर दिया जाता। जांता का पिसा मकई के आंटे की रोटी, चकड़ी में दला गया दाल और मांटी वाले कूंड़े का मठ्ठा ! उसका स्वाद इस उमिर में भी याद है। दरबाजे पर बथान में भर छाती ऊंचे चबुतरा पर माटी की बड़ी नाद, उसके बगल में खूंटा , खूंटे पर बंधा बैल जब सीना तान चभर चभर सानी खाने लगता तो उसके गर्दन में बंधी घंटी और घुंघरु की आवाज़ बड़ी मधुर लगती थी। और हलवाहा, जब खेत जोतते हुए बैल के पुठ्ठे पर हाथ रख कहता , मार लिया भइया, बस हो गया, अब दू आंतर बचल हय, चल तेजी में तो ऐसा लगता था कोई अपने परिवार के बच्चे को पुचकार रहा हो। रेणु जी की तीसरी कसम ( मारे गये गुलफाम ) का हिरामन अपने बैल की जोड़ी से ऐसे ही बतियाता था न ?
 चैत-वैशाख का महीना भी कितना आनन्ददायक था ! मॉर्निंग स्कूल के बाद घर आते ही खटिया पर बस्ता पटक रूखा-सूखा खा कर गाछी की ओर दौड़ पड़ता था आम का टिकोला चुनने। लहालोट पछिया हवा में जब पटापट टिकोला पेंड से गिरता तो चुन-चुन कर चोर खद्धा में जमा करता और फिर झोला भरकर घर लौटता। उससे जो खटाई बनती उसका उपयोग सालो भर चटनी में होता था। तब गेहूं की खेती का उतना प्रचलन नहीं था। कुछ ही लोग पांच-सात कठ्ठा गेहूं बोते थे हमारे गांव में। बांकी लोग पवनी-तिहार, पथ-परहेज के लिए कठ्ठा-दो कठ्ठा ही गेंहू बोते थे। खेती होती थी जौ, केराई, खेसारी और मटर की। तब आज की तरह थ्रेसर नहीं था। जौ की कटनी होती तो बोझा दरबाजे पल लाया जाता। तब दरबाजा भी बड़ा होता था। दरबाजे पर हम बांस के खम्भे का मेहा गारते। मेहा के चारों ओर जौ का बोझा खोल-खोल कर भर ठेहुना मोटा पउर छींट देते। एक-डेढ़ बजते ही वह दौनी करने लायक सूख कर बिल्कुल कड़ा हो जाता, इतना कि उस पर पैर रखते ही कड़कडाहट की आवाज आने लगती।
चैत-वैशाख का महीना भी कितना आनन्ददायक था ! मॉर्निंग स्कूल के बाद घर आते ही खटिया पर बस्ता पटक रूखा-सूखा खा कर गाछी की ओर दौड़ पड़ता था आम का टिकोला चुनने। लहालोट पछिया हवा में जब पटापट टिकोला पेंड से गिरता तो चुन-चुन कर चोर खद्धा में जमा करता और फिर झोला भरकर घर लौटता। उससे जो खटाई बनती उसका उपयोग सालो भर चटनी में होता था। तब गेहूं की खेती का उतना प्रचलन नहीं था। कुछ ही लोग पांच-सात कठ्ठा गेहूं बोते थे हमारे गांव में। बांकी लोग पवनी-तिहार, पथ-परहेज के लिए कठ्ठा-दो कठ्ठा ही गेंहू बोते थे। खेती होती थी जौ, केराई, खेसारी और मटर की। तब आज की तरह थ्रेसर नहीं था। जौ की कटनी होती तो बोझा दरबाजे पल लाया जाता। तब दरबाजा भी बड़ा होता था। दरबाजे पर हम बांस के खम्भे का मेहा गारते। मेहा के चारों ओर जौ का बोझा खोल-खोल कर भर ठेहुना मोटा पउर छींट देते। एक-डेढ़ बजते ही वह दौनी करने लायक सूख कर बिल्कुल कड़ा हो जाता, इतना कि उस पर पैर रखते ही कड़कडाहट की आवाज आने लगती।
टोले में सब के दरबाजे पर तब ऐसा ही पउर लगाया जाता। हमलोग पड़ोस से बैल मांग कर लाते। एक पउर की दौनी के लिए चार या पांच बैल। मेहा में बांधने वाले बैल को मेहिया बैल कहते थे। एक-दूसरे बैल को उसकी गरदानी को रस्सी से जोड़ कर बांधते। सबके अंत में जो बैल बाधा जाता उसी को जब हांकते तो उसी के सहारे सभी बैल मेहा के चारों तरफ घूमने लगता बीच-बीच में बैल को आगे से रोक कर पउर को लाठी से उकटा जाता था। एक पउर पर डेढ़ से दो घंटे दौनी होती फिर दूसरे पउर की बारी आती थी। दो से तीन दिन में जौ का भूसा और अनाज दोनों तैयार। तेज पछिया हवा में ओसौनी होती और चकाचक जौ का दाना भूसा से बाहर हो जाता था। दौनी के दौरान तीन-चार दिनों तक रात में खुले आसमान के नीचे पउर पर सोने में जो आनन्द आता वह आज गद्दे पर सोने में कहां ?
 समय बीतता रहा । खेती-किसानी से जुड़ी हमारी परम्परागत तकनीक गायब होती चली गई। ट्रैक्टर आया तो धीरे-धीरे बैल गायब हो गये। और जब बैल ही नहीं तो बैल से दौनी की कल्पना ही कैसी ? ओखल , मूसल, जांता, चकड़ी, कोठी,बखारी सब गायब हो गया । गांव में धान कूटने और आंटा पीसने की मशीन आई तो कुछ दिनों तक लोग धान मशीन में कुटवाते रहे। अब तो धान तैयार होते ही उसकी बिक्री हो जाती है और हम बड़ी शान से पच्चीस किलो वाले चावल का पैकेट खरीद घर लाने लगे है। गाय-भैंस तो हैं लेकिन दूध दूहने के बाद घरों में नहीं, डेयरी के सेंटर पर ले जाते हैं। कूड़ा का मठ्ठा और कोही का दही आज सपना हो गया। मेरे जेहन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या हम अपनी ही जड़ों से तो नहीं कट गये हैं ? यह परावलम्बन की बेड़ी तो हमने खुद तैयार की है। क्यों और कैसे ? इसका जवाब शोषणमूलक आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में तलाशने की जरूरत है भाई।
समय बीतता रहा । खेती-किसानी से जुड़ी हमारी परम्परागत तकनीक गायब होती चली गई। ट्रैक्टर आया तो धीरे-धीरे बैल गायब हो गये। और जब बैल ही नहीं तो बैल से दौनी की कल्पना ही कैसी ? ओखल , मूसल, जांता, चकड़ी, कोठी,बखारी सब गायब हो गया । गांव में धान कूटने और आंटा पीसने की मशीन आई तो कुछ दिनों तक लोग धान मशीन में कुटवाते रहे। अब तो धान तैयार होते ही उसकी बिक्री हो जाती है और हम बड़ी शान से पच्चीस किलो वाले चावल का पैकेट खरीद घर लाने लगे है। गाय-भैंस तो हैं लेकिन दूध दूहने के बाद घरों में नहीं, डेयरी के सेंटर पर ले जाते हैं। कूड़ा का मठ्ठा और कोही का दही आज सपना हो गया। मेरे जेहन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या हम अपनी ही जड़ों से तो नहीं कट गये हैं ? यह परावलम्बन की बेड़ी तो हमने खुद तैयार की है। क्यों और कैसे ? इसका जवाब शोषणमूलक आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में तलाशने की जरूरत है भाई।